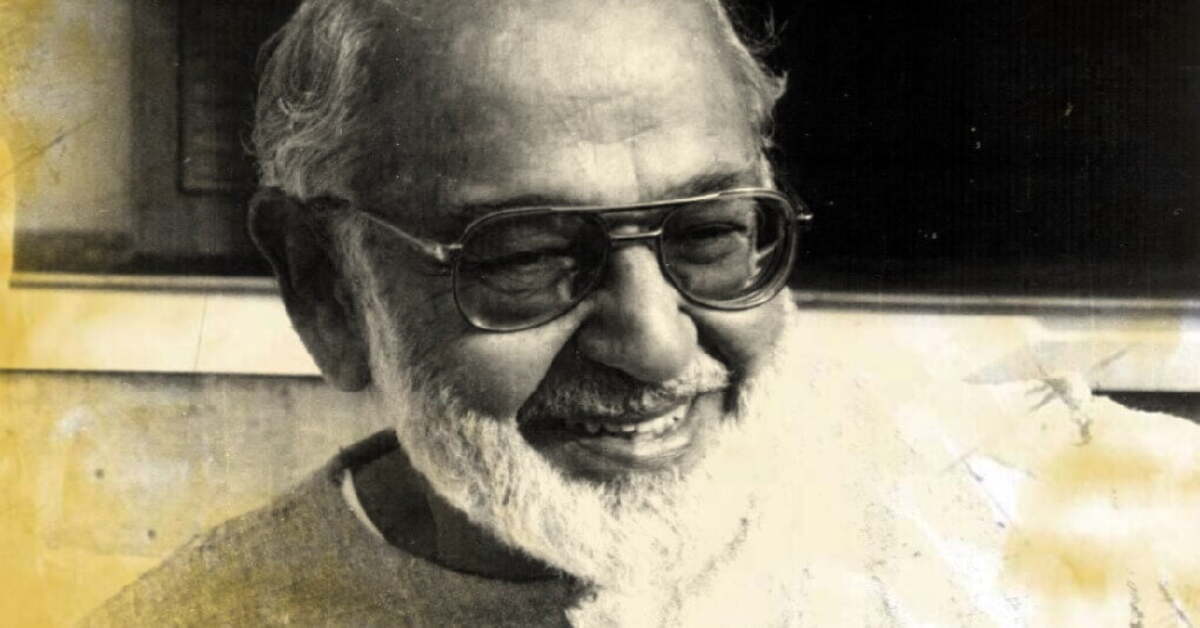हरी बिछली घास।
दोलती कलगी छरहरी बाजरे की।
अगर मैं तुमको ललाती साँझ के नभ की अकेली तारिका
अब नहीं कहता,
या शरद के भोर की नीहार-न्हायी कुँई,
टटकी कली चंपे की, वग़ैरह, तो
नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है
या कि मेरा प्यार मैला है।
बल्कि केवल यही : ये उपमान मैले हो गए हैं।
देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच।
कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है।
मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी :
तुम्हारे रूप के—तुम हो, निकट हो, इसी जादू के—
निजी किस सहज, गहरे बाँध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ—
अगर मैं यह कहूँ—
बिछली घास हो तुम
लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की?
आज हम शहरातियों को
पालतू मालंच पर सँवरी जुही के फूल से
सृष्टि के विस्तार का—ऐश्वर्य का—औदार्य का—
कहीं सच्चा, कहीं प्यारा एक प्रतीक
बिछली घास है,
या शरद की साँझ के सूने गगन की पीठिका पर दोलती कलगी
अकेली
बाजरे की।
और सचमुच, इन्हें जब-जब देखता हूँ
यह खुला वीरान संसृति का घना हो सिमट आता है—
और मैं एकांत होता हूँ समर्पित।
शब्द जादू हैं—
मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है?